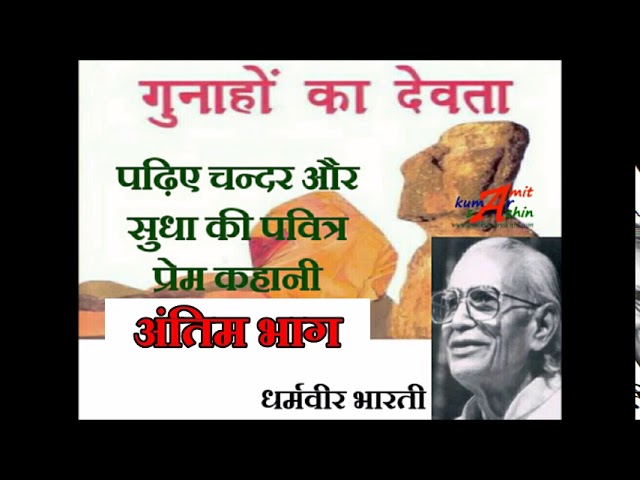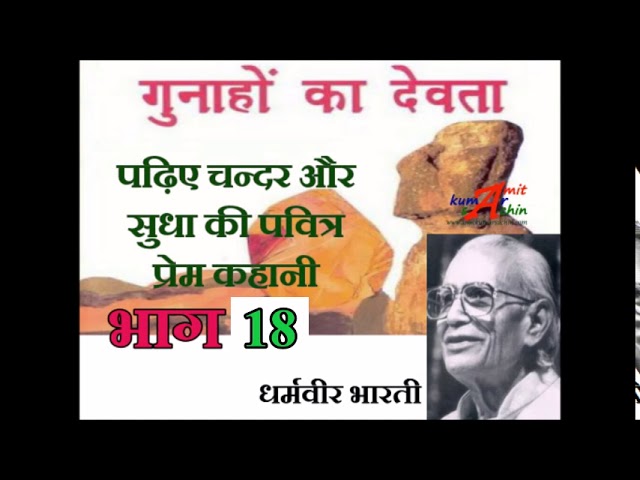गुनाहों के देवता – धर्मवीर भारती
हिंदी साहित्य की लोकप्रिय किताबो की चर्चा की जाये तो धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों के देवता शीर्ष दस पुस्तकों मे माना जाता है | भारत के विभिन्न भाषाओ में इसके करीब सौ संस्करण प्रकाशित हो चुके है | सच बात तो ये है कि इस उपन्यास में एक अजब सा नशा है. आप जितना भी चाहें, एक बार उठाने के बाद इसे रख न सकेंगे. न तो ये कोई थ्रिलर है और ना ही कोई रोमांचक कथा. ये एक साधारण सी पवित्र प्रेम कहानी है – चंदर और सुधा की.. उनके प्यार, उनके बलिदान की… और तो और, यह महज एक काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि इलाहबाद युनिवेर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर की वास्तविक कहानी है!
एक तरफ चंदर, दूसरी ओर सुधा! उन दोनों के अद्वितीय रिश्ते को श्री भारती जी ने इस बखूबी से दर्शाया है, कि आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे ये पात्र आपके चारों ओर मंडरा रहे हों! उन के मन कि उलझनें, अपने मन कि उलझनें लगने लगती हैं! उनके सुख, दुःख, उनकी कठिनायों को हम अपना बना बैठते हैं! और इस कहानी के अंत तक हम में एक छोटी सी झीनी सी आस रहती है कि काश! काश! ऐसा न होता!
गुनाहों के देवता भाग 1
अगर पुराने जमाने की नगर-देवता की और ग्राम-देवता की कल्पनाएँ आज भी मान्य होतीं तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर-देवता जरूर कोई रोमैण्टिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन-सहन में कोई बँधे-बँधाये नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छन्द खुलाव, एक बिखरी हुई-सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियाँ और लखनऊ की सडक़ों से चौड़ी सडक़ें। यार्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइन्स और दलदलों की गन्दगी को मात करने वाले मुहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई सन्तुलन नहीं। सुबहें मलयजी, दोपहरें अंगारी, तो शामें रेशमी! धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे-भरे खेत भी मिलें और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर-देवता स्वर्ग-कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं।
और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार, कार्तिक तथा उधर वसन्त के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नैस्टर्शियम और पैंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है। सिविल लाइन्स हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगातट हो या खुसरूबाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आँचल और लहरों के मिजाज से छेडख़ानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह-सुबह घूमने निकल जाएँ तो इन खुली हुई जगहों की फिजाँ इठलाकर आपको अपने जादू में बाँध लेगी। खासतौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नयी अनुभूति होगी। वसन्त के नये-नये मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली, बाल-सूर्य की अँगुलियाँ सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौंराले गेसुओं को धीरे-धीरे हटाती जाती हैं और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है।
एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक, प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमीं के किनारे-किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटपी के रंग का पश्मीने का लम्बा कोट, जिसका एक कालर उठा हुआ था और दूसरे कालर में सरो की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी, सफेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफेद जरी की पेशावरी सैण्डिलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊँचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते-चलते उसने एक रंग-बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह-रह कर वह उसे सूँघ लेता था।
पूरब के आसमान की गुलाबी पाँखुरियाँ बिखरने लगी थीं और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। ”अरे सुबह हो गयी?” उसने चौंककर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। ”क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गयी?” ”अभी नहीं बाबूजी!” उसने जवाब दिया। वह फिर सन्तोष से बैठ गया और फूलों की पाँखुरियाँ नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियाँ बिखरी थीं और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हलके फालसई रंग के उस फूल पर गहरे बैंजनी डोरे थे।
”हलो कपूर!” सहसा किसी ने पीछे से कन्धे पर हाथ रखकर कहा, ”यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह-सुबह?”
उसने मुडक़र पीछे देखा, ”आओ, ठाकुर साहब! आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इन्तजार कर रहा हूँ।”
”क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली, अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो!”
”हाँ, हाँ, शरीफ लोगों ही के लिए छोड़ रहा हूँ; डॉक्टर शुक्ला की लड़की है न, वह इसकी मेम्बर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा, उसी का इन्तजार भी कर रहा हूँ।”
”डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में हैं?”
”नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में।”
”और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो?”
”नहीं, इकनॉमिक्स में!”
”बहुत अच्छे! तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आये हो?” कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा।
”छिह!” कपूर ने हँसते हुए, कुछ अपने को बचाते हुए कहा, ”यार, तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू सम्बन्ध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ, उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता-लिखता भी हूँ…।”
ठाकुर साहब हँस पड़े, ”अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका-सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो।”
ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बरायनाम विद्यार्थी होते हैं और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे, इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे-खासे रुपये वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकेदार। हँसमुख, फब्तियाँ कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले-
”एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉ. शुक्ला को है! तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं?”
”नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी-न-किसी बहाने मदद की है।”
”अच्छा, आओ, तब तक लोटस-पोंड (कमल-सरोवर) तक ही घूम लें। फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी!”
दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल-सरोवर की ओर चल दिये जो पास ही में बना हुआ था। सीढिय़ाँ चढक़र ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन हैं। छिपकली से दुबले-पतले, बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई-
”कोई प्रेमी हैं, या कोई फिलासफर हैं, देखा ठाकुर?”
”नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं-ये कवि हैं। मैं इन्हें जानता हूँ। ये रवीन्द्र बिसरिया हैं। एम. ए. में पढ़ता है। आओ, मिलाएँ तुम्हें!”
ठाकुर साहब ने एक बड़ा-सा घास का तिनका तोडक़र पीछे से चुपके-से जाकर उसकी गरदन गुदगुदायी। बिसरिया चौंक उठा-पीछे मुडक़र देखा और बिगड़ गया-”यह क्या बदतमीजी है, ठाकुर साहब! मैं कितने गम्भीर विचारों में डूबा था।” और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आँखें बन्द कर बिसरिया बोला, ”आह! कैसा मनोरम प्रभात है! मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी…।”
कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुसकराया और इशारे में बोला, ”है यार शगल की चीज। छेड़ो जरा!”
ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, ”माफ करना, भाई बिसरिया! बात यह है कि हम लोग कवि तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम?”
बिसरिया ने आँखें खोलीं और एक गहरी साँस लेकर बोला, ”मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है? कविता क्यों लिखी जाती है? फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी-संग्रह?”
”बात तो गम्भीर है।” कपूर बोला, ”जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है-प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है, मसलन क्वार-कार्तिक या फागुन-चैत। उसका सम्बन्ध रीढ़ की हड्डी से होता है। और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं, मि. सिबरिया?”
”सिबरिया नहीं, बिसरिया?” ठाकुर साहब ने टोका।
बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, ”क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ…।”
कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, ”अरे भाई, बेकार उलझ गये तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चन्द्रकुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं और आप हैं श्री रवीन्द्र बिसरिया, इस वर्ष एम. ए. में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं।”
कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गम्भीरता से बोला, ”क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं?”
बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ”ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ।” और उठ खड़ा हुआ।
”अरे बैठो-बैठो!” ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया, ”देखो, कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह है कि तुममें इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते। इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते। वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं। मुझसे बराबर तारीफ करते हैं।”
बिसरिया पिघल गया और बोला, ”क्षमा कीजिएगा। मैंने गलत समझा, अब मेरा कविता-संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूँगा।” और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुडक़र बोला, ”अब लोग मेरी कविताओं की इतनी माँग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल ‘त्रिवेणी’ के सम्पादक मिले। कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गये। आखिरकार मैंने आइडेण्टिटी कार्ड उठाकर दे दिया!”
”वाह!” कपूर बोला, ”मान गये आपको हम! तो आप राष्ट्रीय कविताएँ लिखते हैं या प्रेम की?”
”जब जैसा अवसर हो!” ठाकुर साहब ने जड़ दिया, ”वैसे तो यह वारफ्रण्ट का कवि-सम्मेलन, शराबबन्दी कॉन्फ्रेन्स का कवि-सम्मेलन, शादी-ब्याह का कवि-सम्मेलन, साहित्य-सम्मेलन का कवि-सम्मेलन सभी जगह बुलाये जाते हैं। बड़ा यश है इनका!”
बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुँह पर लाकर गम्भीर हो गया।
कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ”तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए न!”
”अभी तो मूड नहीं है।” बिसरिया बोला।
ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले पाँच सालों से जानते थे, वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अत: बोले, ”ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ। ज़रा गंगाजी चलें, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना-पीना रहे तब कविता भी सुनना!”
कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था। फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया।
इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, ”अच्छा, ठाकुर साहब, मुझे तो इजाजत दीजिए। अब चलूँ लाइब्रेरी में। वो लोग आ गये। आप कहाँ चल रहे हैं?”
”मैं ज़रा जिमखाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही।”
”बिल्कुल पक्की!” कपूर बोला और चल दिया।
लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अन्दर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी।
”क्यों सुधा, अन्दर क्यों बैठी हो?”
”तुम्हें ही देख रही थी, चन्दर।” और वह उतर आयी। दुबली-पतली, नाटी-सी, साधारण-सी लड़की, बहुत सुन्दर नहीं, केवल सुन्दर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी।
”चलो, अन्दर चलो।” चन्दर ने कहा।
वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गयी और बोली, ”चन्दर, एक आदमी को चार किताबें मिलती हैं?”
”हाँ! क्यों?”
”तो…तो…” उसने बड़े भोलेपन से मुसकराते हुए कहा, ”तो तुम अपने नाम से मेम्बर बन जाओ और दो किताबें हमें दे दिया करना बस, ज्यादा का हम क्या करेंगे?”
”नहीं!” चन्दर हँसा, ”तुम्हारा तो दिमाग खराब है। खुद क्यों नहीं बनतीं मेम्बर?”
”नहीं, हमें शरम लगती है, तुम बन जाओ मेम्बर हमारी जगह पर।”
”पगली कहीं की!” चन्दर ने उसका कन्धा पकडक़र आगे ले चलते हुए कहा, ”वाह रे शरम! अभी कल ब्याह होगा तो कहना, हमारी जगह तुम बैठ जाओ चन्दर! कॉलेज में पहुँच गयी लड़की; अभी शरम नहीं छूटी इसकी! चल अन्दर!”
और वह हिचकती, ठिठकती, झेंपती और मुड़-मुडक़र चन्दर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अन्दर चली गयी।
थोड़ी देर बाद सुधा चार किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, ”लाओ, मैं ले लूँ!” तो बाँस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, ”सदस्य मैं हूँ। तुम्हें क्यों दूँ किताबें?” और जाकर कार के अन्दर किताबें पटक दीं। फिर बोली, ”आओ, बैठो, चन्दर!”
”मैं अब घर जाऊँगा।”
”ऊँहूँ, यह देखो!” और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, ”देखो, यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेन्स है न। वहीं पढऩे के लिए यह निबन्ध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएँ हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गये हैं। समझे जनाब!” उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गरदन हिलाकर शोख स्वरों में कहा।
कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, ”लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख, इतने पृष्ठ, शाम तक कौन टाइप कर देगा?”
”इसका भी इन्तजाम है,” और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चन्दर के हाथ में देती हुई बोली, ”यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है। टाइपिस्ट। इसके घर मैं तुम्हें पहुँचाये देती हूँ। मुकर्जी रोड पर रहती है यह। उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना।”
”लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी।”
”समझ गये, अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊँ? पापा का काम है यह! चलो, आओ!”
चन्दर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा, ”अरे, चारों कविता की किताबें उठा लायी-समझ में आएँगी तुम्हारे? क्यों, सुधा?”
”नहीं!” चिढ़ाते हुए सुधा बोली, ”तुम कहो, तुम्हें समझा दें। इकनॉमिक्स पढऩे वाले क्या जानें साहित्य?”
”अरे, मुकर्जी रोड पर ले चलो, ड्राइवर!” चन्दर बोला, ”इधर कहाँ चल रहे हो?”
”नहीं, पहले घर चलो!” सुधा बोली, ”चाय पी लो, तब जाना!”
”नहीं, मैं चाय नहीं पिऊँगा।” चन्दर बोला।
”चाय नहीं पिऊँगा, वाह! वाह!” सुधा की हँसी में दूधिया बचपन छलक उठा-”मुँह तो सूखकर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पिएँगे।”
बँगला आया तो सुधा ने महराजिन से चाय बनाने के लिए कहा और चन्दर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी।
वैसे तो यह घर, यह परिवार चन्द्र कपूर का अपना हो चुका था; जब से वह अपनी माँ से झगडक़र प्रयाग भाग आया था पढऩे के लिए, यहाँ आकर बी. ए. में भरती हुआ था और कम खर्च के खयाल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था, तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चन्दर की अँग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉ. शुक्ला उससे अक्सर छोटे-छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तम्भ का काम चन्दर को दिलवा दिया था और उसके बाद चन्दर के लिए डॉ. शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। चन्दर शरमीला लड़का था, बेहद शरमीला, कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश न की थी, लेकिन जब बी. ए. में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक सम्पादक बना दिया था। एम. ए. में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉ. शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गये थे। अगर सच पूछा जाय तो उसके सारे कैरियर का श्रेय डॉ. शुक्ला को था जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ायी और उसको अपने लड़के से बढक़र माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉ. शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाये रखा कि कैसे धीरे-धीरे चन्दर सारी गैरियत खो बैठा; यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बँगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का सम्बन्ध था।
और यह नन्ही दुबली-पतली रंगीन चन्द्रकिरन-सी सुधा। जब आज से वर्षों पहले यह सातवीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आयी थी तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चन्दर की अपनी होती गयी थी, इसे चन्दर खुद नहीं जानता था। जब वह आयी थी तब वह बहुत शरमीली थी, बहुत भोली थी, आठवीं में पढऩे के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे, वह स्कूल नहीं जाती थी। तीन बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और दस साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गाँव में रही थी। अब तेरह वर्ष की होने पर गाँव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गाँव की औरतों ने हाथ नचाना और मुँह मटकाना शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर आठवीं में भर्ती करा दिया। जब वह आयी थी तो आधी जंगली थी, तरकारी में घी कम होने पर वह महराजिन का चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोडक़र न लाने पर अकसर उसने माली को दाँत भी काट खाया था। चन्दर से जरूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चन्दर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब दो साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे और न उससे बोलते थे, तो वह रो-रोकर और सिर पटक-पटककर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चन्दर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डाँटा था, समझाया था, और सुधा, घर-भर से अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़-फोड़ मचाती रहने वाली सुधा, चन्दर की आँख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शान्त हो जाती थी। कब और क्यों उसने चन्दर के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम था, और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने-आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था, दोनों का एक-दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी।
और मजा तो यह था कि चन्दर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गयी थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुँझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई-झगड़ा, सभी की तरफ से हटकर चन्दर की ओर केन्द्रित हो गया था। वह विद्रोहिनी अब शान्त हो गयी थी। इतनी शान्त, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टभाषिणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था, लेकिन चन्दर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था और जब तक वह चन्दर को खिझाकर, छेडक़र लड़ नहीं लेती थी उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब दो दिन तक दोनों मुँह फुलाये रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, ”क्या… चन्दर से लड़ाई हो गयी क्या?” फिर वह मुँह फुलाकर शिकायत करती थी और शिकायतें भी क्या-क्या होती थीं, चन्दर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलीफैंटा (श्रीमती हथिनी) रखा था, या चन्दर ने उसको डिबेट के भाषण के प्वाइंट नहीं बताये, या चन्दर कहता है कि सुधा की सखियाँ कोयला बेचती हैं, और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चन्दर को डाँट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चन्दर के आने पर आँखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, ”कहो, कैसी डाँट पड़ी?”
वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन-सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीजों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसायटियों के मेम्बर हैं, चन्दर के इक्नॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी-बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख-दु:ख कह देते थे। पढ़ाई के साथ-साथ घर का सारा काम-काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शान्त, संयम, गम्भीर और बुजुर्ग थी, मगर अपने पापा और चन्दर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन।
लेकिन हाँ, एक बात थी। उसे जितना स्नेह और स्नेह-भरी फटकारें और स्वास्थ्य के प्रति चिन्ता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े नि:स्वार्थ भाव से वह चन्दर को दे डालती थी। खाने-पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चन्दर का रखती थी और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पागकर वह चन्दर को दे डालती थी। चन्दर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सबका लेखा-जोखा उसे सुधा को देना पड़ता, और जब कभी उसके खाने-पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डाँट खानी ही पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी; और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चन्दर अभी बच्चा था। और कभी-कभी तो सुधा की स्वास्थ्य-चिन्ता इतनी ज्यादा हो जाती थी कि चन्दर बेचारा जो खुद तन्दुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तहान में जब चन्दर कुछ दुबला-सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आयी। और लगी चन्दर से जिद करने कि ”पियो इसे!” जब चन्दर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची।
इसीलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह काँप गयी क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुँह तक दूध भरकर उसमें दो-तीन चम्मच चाय का पानी डाल देती थी और अगर उसने ज्यादा स्ट्रांग चाय की माँग की तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता था। और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या-क्या, और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा और उसके बाद की लम्बी-चौड़ी मनुहार; इस सबसे चन्दर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लायी तो उसे मजबूर होना पड़ा, और बैठे-बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी-सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और दो चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगे, और बेतकल्लुफी से दूधिया चाय का प्याला चन्दर के सामने खिसकाकर बोली, ”पीजिए, नाश्ता आ रहा है।”
चन्दर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीरसागर नजर आया तो उसने हारकर प्याला रख दिया।
”क्यों, पीते क्यों नहीं?” सुधा ने अपना प्याला रख दिया।
”पीएँ क्या? कहीं चाय भी हो?”
”तो और क्या खालिस चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए।”
”तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूँ या रिसर्च। न ऐसी चाय मुझे पसन्द, न ऐसा दिमागी काम!”
”लो, आपको विश्वास नहीं होता। मेरी क्लासफेलो है गेसू काजमी; सबसे तेज लड़की है, उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबालकर देती है।”
”क्या नाम है तुम्हारी सखी का?”
”गेसू!”
”बड़ा अच्छा नाम है!”
”और क्या! मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम!”
”जरूर-जरूर,” मुँह बिचकाते हुए चन्दर ने कहा, ”और उतनी ही काली होगी, जितने काले गेसू।”
”धत्, शरम नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए!”
”और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब?”
”तब क्या! वे तो सब हैं ही बुरे! अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ,” और वह प्लेट में छील-छीलकर सन्तरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए सन्तरे को नीचे से उठाने लगी कि चन्दर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शान्त चित्त से पीने लगा। सन्तरे की फाँकें उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूँट चाय ली तो वह चौंककर बोली, ”अरे, यह क्या हुआ?”
”कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है!” चन्दर ने ठाठ से चाय घूँटते हुए कहा। सुधा कुढ़ गयी। कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चन्दर ने घड़ी देखी।
”अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है।”
”बस यहाँ तो एक मिनट बैठना बुरा लगता है आपको! हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए न!”
”अरे, तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है?”
”करनी क्यों नहीं है। आज तो गेसू को मोटर पर लेते हुए तब जाना है!”
”तुम्हारी गेसू और कभी मोटर पर चढ़ी है?”
”जी, वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है, उसके यहाँ दो मोटरें हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं।”
”अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की?”
”अहा हा, गेसू के यहाँ दावत खाएँगे! इसी मुँह से! जनाब उसकी शादी भी तय हो गयी है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाय।”
”छिह, बड़ी खराब लड़की हो! कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा?”
सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय-भरी मुसकान से उसकी ओर देखा। चन्दर ने झेंपकर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चन्दर का कन्धा पकडक़र बोली-”अरे उदास हो गये, नहीं भइया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएँगे, घबराते क्यों हो!” और एक मोटी-सी इकनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, ”लो, इस मुटकी से ब्याह करोगे! लो बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबन्ध ले आऊँ, टाइप कराने वाला।”
चन्दर ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। ”हाय रे!” सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुँह बनाते हुए कहा, ”लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप?” और वह चली गयी! डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबन्ध उठा लायी और बोली, ”लो, यह निबन्ध की पाण्डुलिपि है।” उसके बाद चन्दर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, ”शाम को आओगे?”
”न!”
”अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे। तुम चुपचाप पढऩा। जब रात को पापा आ जाएँ तो उन्हें निबन्ध की प्रतिलिपि देकर चले जाना!”
”नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ।”
”तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गयी है, मास्टर ढूँढ़ दो हमें।”
”नहीं, ये सब झूठी बात है। हम कल सुबह आएँगे।”
”अच्छा, तो सुबह जल्दी आना और देखो, मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुकर्जी रोड पहुँचा देगा।”
वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गयी कि फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, ”लो, यह लिफाफा तो भूल ही गये थे। पापा ने लिख दिया है। उसे दे देना।”
”अच्छा।” कहकर फिर चन्दर चला कि फिर सुधा ने पुकारा, ”सुनो!”
”एक बार में क्यों नहीं कह देती सब!” चन्दर ने झल्लाकर कहा।
”अरे बड़ी गम्भीर बात है। देखो, वहाँ कुछ ऐसी-वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ दो बड़े-बड़े बुलडॉग हैं।” कहकर उसने गाल फुलाकर, आँख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनायी कि चन्दर हँस पड़ा। सुधा भी हँस पड़ी।
ऐसी थी सुधा, और ऐसा था चन्दर।